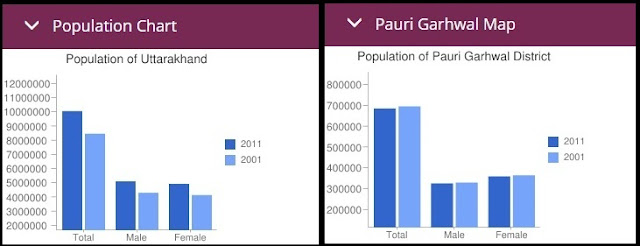|
| सिलबट्टा यानि सिलौटा, सिल्वाटु : पहाड़ी रसोईघरों का अभिन्न अंग। स्वाद और स्वास्थ्य के लिये भी जरूरी है सिलौटा का उपयोग। फोटो : रविकांत घिल्डियाल |
सिलोटु, सिल्वाटु, सिळवाटू, सिलौटा, सिलोटी या सिलबट्टा। मसालों को पीसने की इस पारंपरिक 'मशीन' से आप सभी परिचित होंगे। अब भी गांवों में इसका उपयोग किया जाता है। सिलबट्टा यानि पत्थर का ऐसा छोटा चोकौर या लंबा टुकड़ा जिससे मसाला आदि पीसा जाता है। सिल और पीसने का लोढ़ा। जो बड़ी सिल होती है उसे सिलौटा और जो छोटी सिल होती है उसे सिलोटी कहा जाता है। सिल और बट्टा होते अलग अलग हैं लेकिन एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं है। सिल जमीन पर रखा पत्थर जिस पर बट्टे से अनाज पीसा जाता है। मिस्र की पुरानी सभ्यताओं में जो सिल मिला था वह बीच में थोड़ा दबा हुआ है। आज भी सिल का बीच का हिस्सा मामूली गहरा होता है। बट्टे को दोनों हाथों से पकड़कर और घुटनों के बल बैठकर सिल पर अनाज या मसाले पीसे जाते हैं।
सिलोटु में पीसे गये मसालों से सब्जी का स्वाद ही बदल जाता है और यह भोजन स्वास्थ्य के लिये भी उत्तम होता है। लेकिन आजकल पिसे हुए मसालों का जमाना है या फिर सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले ली है। सिलोटु घर के किसी कोने में दुबका हुआ है। वही सिलबट्टा जो हजारों वर्षों से भारत ही नहीं मिस्र तक की सभ्यताओं का अहम अंग रहा है। आयुर्वेद पुरोधा वाग्भट्ट ने अपने चौथे सिद्धांत से हमें सिलोटा के महत्व का पता चल जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, ''कोई भी कार्य यदि अधिक गति से किया जाता है तो उससे वात (शरीर के भीतर की वह वायु जिसके विकार से अनेक रोग होते हैं) उत्पन्न होता है।'' कहने का मतलब है कि यदि हम किसी खाद्य सामग्री को बहुत तेजी से पीसकर तैयार करते हैं तो उसके सेवन से वात पैदा होता है। भारत में वैसे भी 70 प्रतिशत रोग वातजनित हैं। रसोई में जो भी प्रक्रियाएं अपनायी जाएं वे गतिमान और सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए। अगर आटा धीरे धीरे पिसा हुआ होता है यानि उसे घर में पीसा जाता है तो वह कई गुणों से भरपूर होता है लेकिन चक्की में आटा बहुत तेजी से पीसा जाता है। यही सूत्र मसालों पर भी लागू होता है और इसलिए सिलबट्टा में पीसे गये मसालों को अधिक गुणकारी माना जाता है। असल में घर की चक्की और सिलबट्टा के उपयोग से भोजन का स्वाद बढ़ने के साथ स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और इनके उपयोग करने वाले का भी समुचित व्यायाम हो जाता है। लेकिन अब बिजली से चलने वाली चक्की और मिक्सी के प्रयोग से भोजन का स्वाद कम हो गया और भोजन भी पौष्टिकता से भरपूर नहीं है। लोग मिक्सी से भोजन की पौष्टिकता पर पड़ रहे कुप्रभावों से भी अवगत हैं लेकिन इसके बावजूद दौड़ती भागती जिंदगी में मिक्सी रानी का पूरा दबदबा है। उसके सामने सिलबट्टा 'बेचारा' बन गया है जबकि गुणों के मामले में वह बादशाह है।
आटे की चक्की ने तो पहाड़ी गांवों में भी बहुत पहले प्रवेश कर दिया था लेकिन सिलोटा यानि सिलबट्टा का ठाठ बाट बने रहे। सिलबट्टा को रखने की एक नियत जगह होती थी जिसे हमेशा साफ सुथरा रखा जाता था। सिलबट्टा को इस्तेमाल से पहले और बाद में अच्छी तरह से धोया और पोछा जाता था और बाद में दीवार के सहारे से शान से खड़ा कर दिया जाता था। वरिष्ठ पत्रकार और उत्तराखंड़ी परंपरों के जानकार श्री विवेक जोशी के शब्दों में, ''आधुनिक मिक्सर की इस दादी के कभी बड़े राजसी ठाठ थे। इनकी नियत जगह होती, इनको इस्तेमाल से पहले और बाद में धो पोछकर दीवार के सहारे टिका दिया जाता। कुछ तो धूप आरती भी करते। समझा जाता था कि घर की खुशहाली के लिये यह सगुन है। हो भी क्यों ना..सेहत का राज इससे जुड़ा था। एक कहानी है..एक दादी के मरने के बाद कुछ ना मिला सिवाय एक संदूक के। लालची बहुओं ने खोला तो उसमें था 'सिलबट्टा '। दादी का संदेश साफ था लेकिन बहुओं ने उसे फेंक दिया और संदूक को चारपाई के नीचे रख दिया। तब से यही होता आ रहा है..सेहत फेंक दी गयी और कलह को चारपाई के नीचे जगह मिल गयी।''
मसालों से लेकर लूण (नमक) पीसने, आलू या मूली की थेंच्वाणि (आलू, मूली या अन्य तरकारी को कुचलकर बनायी गयी रसदार सब्जी), दाल पीसने या दाल और किसी अन्य अनाज को दुदळो करने, दाल के पकोड़े (भूड़ा) बनाने आदि के लिये सिलबट्टा का उपयोग किया जाता है। सिलबट्टे पर बनायी गयी चटनी जैसा स्वाद मिक्सी की चटनी में कभी नहीं आ सकता है।
 |
| सिलबट्टे पर पिसे मसालों की महक से चेहरे पर खिल उठती है मुस्कान : फोटो रविकांत घिल्डियाल |
सिलबट्टा के उपयोग के फायदे
-- सिलबट्टा पत्थर से बनता है। पत्थर में कई बार के खनिज भी होते हैं और इसलिए सिलबट्टा में मसाले पीसने से ये खनिज भी उनमें शामिल होते रहते हैं जिससे न सिर्फ स्वाद में वृद्धि होती है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिये भी उत्तम होता है।
-- सिलबट्टे में मसाले पीसते वक्त व्यायाम होता है उससे पेट बाहर नही निकलता। इससे विशेषकर इससे यूटेरस की बहुत अच्छी कसरत हो जाती है। महिलाएं पहले हर रोज सिलबट्टे का उपयोग करती थी और इससे तब बच्चे की सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत नहीं पडती थी। मतलब सिलबट्टे का उपयोग किया तो जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ।
-- सिलबट्टा आदि में सब कुछ धीरे धीरे पिसता है तथा अनाज या मसाला जरूरत से ज्यादा सूक्ष्म भी नहीं होता है। इससे वात संबंधी रोग नहीं होते हैं। मिक्सी आदि में न केवल तेजी से पिसाई होती है बल्कि वह अतिसूक्ष्म भी हो जाता है। इस तरह से वह वातकारक है।
-- सिलबट्टा का उपयोग करने से मिक्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे बिजली का खर्च भी कम होगा।
सिलबट्टा का धार्मिक महत्व
सिलबट्टा सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है बल्कि उसका धार्मिक महत्व भी है। गांवों में हर किसी के घर में सिलबट्टा होता है। श्री विवेक जोशी ने बताया, ''जिसके घर विवाह होता है वह एक सिल जरूर खरीदता है। पाणीग्रहण के समय "शिला रोहण" के लिए सिलबट्टा गरीब से गरीब व्यक्ति खरीदता है। इसे पार्वती का प्रतीक माना जाता है और यह बेटी की सखी के रूप में उसके साथ ससुराल जाता है।''
विभिन्न तरह के यज्ञों में भी सिलबट्टा के उपयोग की बात सामने आती है। इसे दषद उपल नाम से जाना जाता है। यज्ञ में अन्न सिद्ध करने के जिन साधनों का वर्णन है उनमें सूप, चलनी, ओखली, मूसल आदि के साथ सिलबट्टा भी शामिल है।
पहाड़ों में यह भी मान्यता है कि सिल और बट्टा एक साथ बेचा और खरीदा नहीं जाता है। बट्टे को शिव का और सिल को पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इन दोनों को जन्म देने वाला "शिल्पकार" इनका पिता समान होता है और इसलिए वह दोनों को एक साथ नहीं देता। पहले दोनों में किसी एक को लेना पड़ता था फ़िर कुछ दिन बाद इसकी जोड़ी पूरी करनी पड़ती है। यह भी कहा जाता है कि दीपावली पूजन के बाद चूने या गेरू में रूई भिगोकर चक्की, चूल्हा, सिलबट्टा और सूप पर तिलक करना चाहिए। उत्तराखंड के कुमांऊ संभाग में ग्वल या गोलू देवता की कहानी भी सिलबट्टा से जुड़ी है।
'घसेरी' का आपसे अनुरोध है कि घर में मसाले आदि पीसने के लिये अधिक से अधिक सिलौटा का उपयोग करने की कोशिश करिये। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन फायदे भी तो अनेक हैं। उम्मीद है कि हमारे गांव घरों में सिलौटा, सिलोटु या सिलोटी अपना स्थान बरकरार रखेगी। आपका धर्मेन्द्र पंत
------- घसेरी के यूट्यूब चैनल के लिये क्लिक करें घसेरी (Ghaseri)
------- Follow me on Twitter @DMPant
------- घसेरी के यूट्यूब चैनल के लिये क्लिक करें घसेरी (Ghaseri)
------- Follow me on Twitter @DMPant